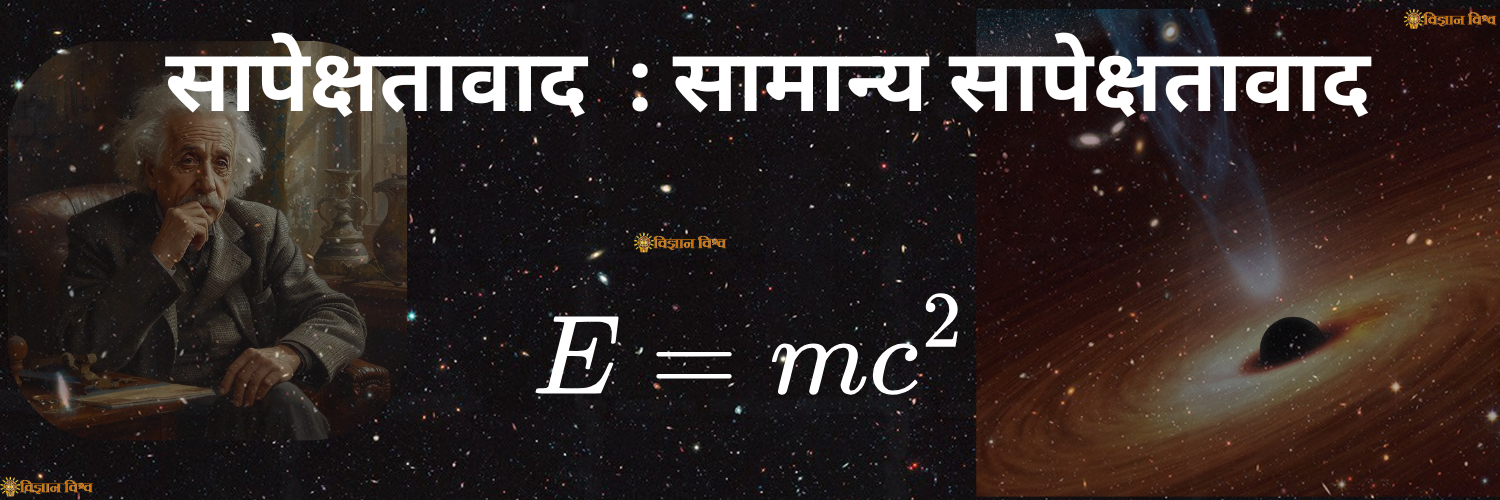---मेहेर वान
 जगजीत सिंह की आवाज़ कब जिंदगी की हमसफ़र बन गयी, पता ही नहीं चला।
कभी इसी आवाज़ को दादा के रेडियो और पापा के टेप-रिकॉर्डर पर सुना था। जब स्कूल में
था तो जगजीत की ग़ज़लों के अर्थ अनबूझे से लगते थे, जिन्हें महसूस करने के लिये शायद
न तो हमारे लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ थी न हमारा संघर्ष उन भावनाओं और एहसासों से
मेल खाता था। धीरे-धीरे समय के साथ अनुभव और एहसास बदलते गये, तो जगजीत सिंह की ग़ज़लें
क़रीब आती गयीं। इसका कारण सिर्फ़ ग़ज़लों के बेहतरीन शब्द ही नहीं थे, जो मध्यवर्गीय संघर्ष
और भावनाओं के ज्वार-भाटों को किनारा देते हुये प्रतीत होते थे। उन शब्दों को सुरों
से सजाने वाली आवाज़ भी उतनी ही असरदार और अपनापे का एहसास कराने वाली थी कि जगजीत के
चाहने वालों में उम्र का फ़र्क मिट जाता है। शायद यही कारण है कि, हर कोई अपने-अपने
स्तर पर जगजीत की ग़ज़लों से जुड़ने का कारण तलाश लेता है। जगजीत सिंह ने ग़ज़ल गायिकी को
उस समय एक नयी दिशा दी, जब ग़ज़लों के चाहने वाले लगातार कम हो रहे थे। ६० के दशक में
ग़ज़ल गायिकी में शास्त्रीय संगीत का प्रभाव ज़्यादा था। उन्होंने ग़ज़ल गायिकी को परंपरागत
संगीत और गायन से अलग करते हुये, उसमें पार्श्व संगीत का उपयुक्त समायोजन करते हुये
नयी तरह से ग़ज़ल गाना शुरु किया। ग़ज़ल को सुगम और सुग्राह्य बनाने के लिये उन्होंने अपेक्षाकृत
सरल शब्दों वाली रचनायें भी गायन के लिये चुनीं, उनका यह प्रयोग सफ़ल रहा और इससे आम
लोगों में ग़ज़ल की पहुँच लगातार बढ़ती गयी।
जगजीत सिंह की आवाज़ कब जिंदगी की हमसफ़र बन गयी, पता ही नहीं चला।
कभी इसी आवाज़ को दादा के रेडियो और पापा के टेप-रिकॉर्डर पर सुना था। जब स्कूल में
था तो जगजीत की ग़ज़लों के अर्थ अनबूझे से लगते थे, जिन्हें महसूस करने के लिये शायद
न तो हमारे लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ थी न हमारा संघर्ष उन भावनाओं और एहसासों से
मेल खाता था। धीरे-धीरे समय के साथ अनुभव और एहसास बदलते गये, तो जगजीत सिंह की ग़ज़लें
क़रीब आती गयीं। इसका कारण सिर्फ़ ग़ज़लों के बेहतरीन शब्द ही नहीं थे, जो मध्यवर्गीय संघर्ष
और भावनाओं के ज्वार-भाटों को किनारा देते हुये प्रतीत होते थे। उन शब्दों को सुरों
से सजाने वाली आवाज़ भी उतनी ही असरदार और अपनापे का एहसास कराने वाली थी कि जगजीत के
चाहने वालों में उम्र का फ़र्क मिट जाता है। शायद यही कारण है कि, हर कोई अपने-अपने
स्तर पर जगजीत की ग़ज़लों से जुड़ने का कारण तलाश लेता है। जगजीत सिंह ने ग़ज़ल गायिकी को
उस समय एक नयी दिशा दी, जब ग़ज़लों के चाहने वाले लगातार कम हो रहे थे। ६० के दशक में
ग़ज़ल गायिकी में शास्त्रीय संगीत का प्रभाव ज़्यादा था। उन्होंने ग़ज़ल गायिकी को परंपरागत
संगीत और गायन से अलग करते हुये, उसमें पार्श्व संगीत का उपयुक्त समायोजन करते हुये
नयी तरह से ग़ज़ल गाना शुरु किया। ग़ज़ल को सुगम और सुग्राह्य बनाने के लिये उन्होंने अपेक्षाकृत
सरल शब्दों वाली रचनायें भी गायन के लिये चुनीं, उनका यह प्रयोग सफ़ल रहा और इससे आम
लोगों में ग़ज़ल की पहुँच लगातार बढ़ती गयी।
जगजीत सिंह का संगीत में बचपन से ही रुझान था और वे अपने पैतृक
गाँव श्रीगंगा-नगर में पं०छगनलाल शर्मा से संगीत की शिक्षा लेना शुरु कर चुके थे। इसके
बाद, महान गायक तानसेन के सैनिया घराना के गायक उस्ताद जमाल खान के यहाँ भी उन्होंने
छः साल तक ठुमरी, खयाल ध्रुपद और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। संगीत
की बारीकियाँ उन्होंने यहीं सीखीं। इसके साथ ही जगजीत सिंह ने इतिहास में कुरुक्षेत्र
विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई भी की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तत्कालीन
कुलपति सूरजभान उनकी गायन प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने
ही जगजीत सिंह को गायन में अपना कैरियर बनाने कि लिये प्रेरित करते हुये बम्बई जाने
की सलाह दी थी। जगजीत सिंह, अपने परिवार में जीत सिंह के नाम से जाने जाते थे, और गायिकी
की शुरुआत में वे जगमोहन के नाम से गाते थे, बाद में वे अपना नाम बदल कर जगजीत सिंह
के नाम से गाने लगे। बम्बई में फ़िल्मों में पार्श्व गायन्के लिये आये थे मगर गायन के
क्षेत्र में उनकी शुरुआत विज्ञापनों में गाये जाने वाले “जिंगल्स” से हुयी। सुरेश अमीन
की गुज़राती फ़िल्म “धरती ना छोरू” में उन्हें सबसे पहले ब्रेक मिला। विज्ञापनों में
जिंगल्स गाते हुये उनकी भेंट चित्रा सिंह से हुयी, चित्रा सिंह भी गायन से जुड़ी हुयीं
थीं। बाद में इस जोड़ी ने कई बेहतरीन दिल को छू लेने वाली सुरीली धुनों से सजी गज़लों
से भारतीय संगीत से नवाज़ा।
१९७० का दौर नूर जहाँ, मल्लिका पुखराज, बड़े ग़ुलाम अली ख़ाँ, मेंहदी
हसन, तलत मेहमूद, और बेग़म अख़्तर की ग़ज़ल गायिकी का दौर था। सन १९७६ में जगजीत सिंह ने
अर्द्ध-शास्त्रीय भारतीय संगीत पर आधारित ग़ज़ल-संग्रह “द अन्फ़ोरगेटबल्स” के नाम से निकाला,
जिसकी परंपरागत आलोचकों ने ग़ज़ल गायन की संरचना को बदलने के कारण काफ़ी निन्दा भी की।
इसके बावजूद यह ग़ज़ल संग्रह अपनी धुनों के सुरीलेपन और जगजीत की ताज़ी मखमली आवाज के
कारण जनता में काफ़ी पसन्द किया गया। इस संग्रह ने ग़ैर-फ़िल्मी संगीत के कैसेटों की बिक्री
के कीर्तिमान स्थापित किये। १९८० के ही दशक में उनकी दो फ़िल्में आयीं- “अर्थ” और “साथ-साथ”
जिसके गीतों से सुनने वालॊं को आज भी उतना ही प्यार है जितना कि उस दौर में था। इसके
बाद जगजीत सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उनके लगातार ग़ज़ल संग्रह आते रहे
जिनमें उनका ग़ज़ल-चयन, धुन-निर्माण, और गायन शैली का संगम इतना बेमिसाल रहा कि संगीत
के चाहने वालों ने उन्हें सर आँखों पर लिया। उनके प्रमुख संग्रहों में सर्च इनसाइट,
मिराज, विज़न, कहकशाँ, लव इज़ ब्लाइंड, चिराग, मरासिम, फ़ेस टू फ़ेस, आइना, वादा, सहर
, लम्हे और कोई बात चले आदि बेहद पसन्द किये गये। इनमें से १९९० के के पहले के लगभग
सभी ग़ज़ल संग्रह उन्होंने चित्रा जी के साथ गाये। चित्रा जी के साथ उनका अंतिम संग्रह
आया- “समवन सम्व्हेयर” (कोई कहीं) और इसके
बाद अपने इकलौते बेटे की असमय मौत के कारण चित्रा जी ने गायन से संन्यास ले लिया। इस
के बाद लता मंगेशकर जी के साथ उनका एक अल्बम
आया “सजदा”, यह अल्बम बहुत ही सुरीली धुनों पर आधारित है और बहुत चर्चित भी हुआ। यहाँ
उनके एक और अल्बम को याद करना ज़रूरी है। १९९० की शुरुआत में “बियॉन्ड टाइम” अल्बम आया
जिसमें उन्होंने चित्रा जी के साथ गाया। यह अल्बम मल्टीट्रेक रिकॉर्डिंग तकनीक पर रिकॉर्ड
हुआ था जो कि उस समय शायद भारतीय ग़ैर-फ़िल्मी गायकों की पहुँच से काफ़ी दूर था। इसमें
प्रचलित सांगीतिक उपकरणॊं के सुरों के इतर भी कुछ आवाज़ें डाली गयीं थीं। जगजीत सिंह
ने मिर्ज़ा ग़ालिब, फ़िराक़ गोरखपुरी, क़तील शिफ़ाई, गुलज़ार और निदा फ़ाज़ली तक के समय के शायरों
के कलामों को अपनी आवाज़ दी। उनकी गायी, बहादुर शाह ज़फ़र की ग़ज़ल “लगता नहीं है दिल मेरा..”
काफ़ी चर्चित हुयी थी। जगजीत सिंह के पंजाबी लोक संगीत में योगदान को भी भुलाया नहीं
जा सकता।
 जगजीत सिंह की गायन-शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने
ग़ज़ल को आम लोगों के स्तर तक उतारा, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने
ग़ज़ल की गम्भीरता को वैसे ही बनाये रखा जैसे कि वह पहले थी। उन्होंने ग़ज़ल को सरल और
सुगम और अधिक सुरीला तो बनाया ताकि जनता और बेहतरी से ग़ज़ल को समझ और महसूस कर सके,
लेकिन ग़ज़ल गायिकी का सरलीकरण नहीं होने दिया। शायद यही प्रमुख कारण है जिसके लिये जगजीत
सिंह लम्बे समय तक याद किये जायेंगे। ज़िंदगी की कठिन पहेली को समझने में आसक्ति और
अनासक्ति के बीच बना जो सूफ़ियाना अंदाज़ होता है वह इस आवाज़ में न जाने कितनी रंगतों
के साथ मुखर हो रहा था। “न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बन्धन..” जैसे शब्दों को
हिन्दी फ़िल्मों के गानों में न जाने कितनी बार दोहराया गया है लेकिन जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत सुनने पर न जाने क्यों दिल की
अन्तिम गहराइयों तक जाता है, दरअसल यह उनकी आवाज़ और उनके एहसास ही थी जो कि शब्दों
को उनके बृहद अर्थ देते थे। यह बाद भी विचारणीय है कि तलत महमूद, किशोर कुमार, महेंद्र
कपूर, हेमंत कुमार जैसे प्रभावशाली गायकों के होते हुये ७० और ८० के दशक में जगजीत
का उदय कैसे हुआ? ये वह दौर था जब फ़िल्मी संगीत तेज़ी से बीट पर आधारित पश्चिमी संगीत
से प्रभावित हो रहा था। गानों में शोर और कोलाहल से युक्त बीट वाला संगीत दिया जा रहा
था। जगजीत सिंह की धुनों का सुरीलापन और माधुर्य तथा आवाज़ का मखमली अंदाज़ संगीत सुनने
वालों को ऐसे समय में बेहतर विकल्प प्रदान करता था। जगजीत सिंह की आवाज़ शास्त्रीय और
अर्द्ध-शास्त्रीय संगीत की परम्पराऒं से बंधी तो हुयी थी मगर अपनी मौलिकता भी लिये
हुयी थी। उनकी सफ़लता का कारण शायद यही है कि उन्होंने शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत
को बहुत ही करीने से साथ साधकर पेश किया। जगजीत सिंह ने ग़ज़लॊं का चयन भी बहुत बेहतर
ढ़ंग के साथ किया। उनकी गायी ग़ज़लें हमेशा साधारण जीवन के संघर्षों के साथ-साथ चलती रहीं।
शहरीकरण के दौर में गायी गयी ग़ज़ल ”ये शहर भी कितना अजीब है, न कोई दोस्त है न कोई रक़ीब
है..” को याद कीजिये, ये वही समय था जब लोगों ने शहरों की तरफ़ भागना शुरु किया था।
रोज़गार और नौकरी की तलाश में युवा शहरों की तरफ़ भाग रहे थे। ये युवा अपने घर-बार, गाँव,
कस्बे छोड़कर शहरआकर आर्थिक रूप से अशक्त तो हो रहे थे लेकिन छूटते साँस्कृतिक संसार
और बिखरते रिश्तों के अकेलेपन में ये ग़ज़लें उनकी तन्हाई और अकेलेपन में साथी बन रहीं
थीं। “तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो…” जैसी ग़ज़लॊं को अपने निराले अंदाज़ और एहसासॊं के
समन्दर से बनी मखमली आवाज़ से सजाकर उन्होंने लोगों के संघर्ष और विजय-पराजय के दुखों-सुखों
को किनारा दिया। जगजीत सिंह गायकी के साथ हमेशा प्रयोग करते रहे। टीवी सीरियल मिर्ज़ा
ग़ालिब में नसीरुद्दीन शाह के बेहतरीन अभिनय और जगजीत की बेमिसाल गायकी से इस टीवी सीरियल
में मिर्ज़ा ग़ालिब के चरित्र की जटिलतायें और बेहतर ढ़ंग से सामने आ सकीं। वस्तुतः, यह
एक तरह की प्रयोगधर्मिता और नया करने की कोशिश भी थी जो जगजीत को अपने अन्य समकालीनों
से अलग करती थी।
जगजीत सिंह की गायन-शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने
ग़ज़ल को आम लोगों के स्तर तक उतारा, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने
ग़ज़ल की गम्भीरता को वैसे ही बनाये रखा जैसे कि वह पहले थी। उन्होंने ग़ज़ल को सरल और
सुगम और अधिक सुरीला तो बनाया ताकि जनता और बेहतरी से ग़ज़ल को समझ और महसूस कर सके,
लेकिन ग़ज़ल गायिकी का सरलीकरण नहीं होने दिया। शायद यही प्रमुख कारण है जिसके लिये जगजीत
सिंह लम्बे समय तक याद किये जायेंगे। ज़िंदगी की कठिन पहेली को समझने में आसक्ति और
अनासक्ति के बीच बना जो सूफ़ियाना अंदाज़ होता है वह इस आवाज़ में न जाने कितनी रंगतों
के साथ मुखर हो रहा था। “न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बन्धन..” जैसे शब्दों को
हिन्दी फ़िल्मों के गानों में न जाने कितनी बार दोहराया गया है लेकिन जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत सुनने पर न जाने क्यों दिल की
अन्तिम गहराइयों तक जाता है, दरअसल यह उनकी आवाज़ और उनके एहसास ही थी जो कि शब्दों
को उनके बृहद अर्थ देते थे। यह बाद भी विचारणीय है कि तलत महमूद, किशोर कुमार, महेंद्र
कपूर, हेमंत कुमार जैसे प्रभावशाली गायकों के होते हुये ७० और ८० के दशक में जगजीत
का उदय कैसे हुआ? ये वह दौर था जब फ़िल्मी संगीत तेज़ी से बीट पर आधारित पश्चिमी संगीत
से प्रभावित हो रहा था। गानों में शोर और कोलाहल से युक्त बीट वाला संगीत दिया जा रहा
था। जगजीत सिंह की धुनों का सुरीलापन और माधुर्य तथा आवाज़ का मखमली अंदाज़ संगीत सुनने
वालों को ऐसे समय में बेहतर विकल्प प्रदान करता था। जगजीत सिंह की आवाज़ शास्त्रीय और
अर्द्ध-शास्त्रीय संगीत की परम्पराऒं से बंधी तो हुयी थी मगर अपनी मौलिकता भी लिये
हुयी थी। उनकी सफ़लता का कारण शायद यही है कि उन्होंने शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत
को बहुत ही करीने से साथ साधकर पेश किया। जगजीत सिंह ने ग़ज़लॊं का चयन भी बहुत बेहतर
ढ़ंग के साथ किया। उनकी गायी ग़ज़लें हमेशा साधारण जीवन के संघर्षों के साथ-साथ चलती रहीं।
शहरीकरण के दौर में गायी गयी ग़ज़ल ”ये शहर भी कितना अजीब है, न कोई दोस्त है न कोई रक़ीब
है..” को याद कीजिये, ये वही समय था जब लोगों ने शहरों की तरफ़ भागना शुरु किया था।
रोज़गार और नौकरी की तलाश में युवा शहरों की तरफ़ भाग रहे थे। ये युवा अपने घर-बार, गाँव,
कस्बे छोड़कर शहरआकर आर्थिक रूप से अशक्त तो हो रहे थे लेकिन छूटते साँस्कृतिक संसार
और बिखरते रिश्तों के अकेलेपन में ये ग़ज़लें उनकी तन्हाई और अकेलेपन में साथी बन रहीं
थीं। “तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो…” जैसी ग़ज़लॊं को अपने निराले अंदाज़ और एहसासॊं के
समन्दर से बनी मखमली आवाज़ से सजाकर उन्होंने लोगों के संघर्ष और विजय-पराजय के दुखों-सुखों
को किनारा दिया। जगजीत सिंह गायकी के साथ हमेशा प्रयोग करते रहे। टीवी सीरियल मिर्ज़ा
ग़ालिब में नसीरुद्दीन शाह के बेहतरीन अभिनय और जगजीत की बेमिसाल गायकी से इस टीवी सीरियल
में मिर्ज़ा ग़ालिब के चरित्र की जटिलतायें और बेहतर ढ़ंग से सामने आ सकीं। वस्तुतः, यह
एक तरह की प्रयोगधर्मिता और नया करने की कोशिश भी थी जो जगजीत को अपने अन्य समकालीनों
से अलग करती थी।
१० अक्टूबर, २०११ को यह महान संगीतज्ञ हमें छोड़कर विदा
हो गया, लेकिन ज़िंदगी की घनी धूप में उनकी ग़ज़लें घना साया बनकर हमारे बीच हमेशा ज़िंदा
रहेंगी। ये अलग बात है कि उनके जाने के बाद हमें ये आभास हो- “तुम चले जाओगे तो हम सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या
पाया…”।
******************************************